 कल उड़न तश्तरी पर समीर भाई के सुभाषित का आनंद ले रहा था कि उनके एक सुभाषित पर नज़र पड़ी ..”प्रशंसा और आलोचना में वही फर्क है जो सृजन और विंध्वस में “ अरे.. मैने कहा यह तो मेरे ब्लॉग के काम की चीज़ है । याद आया अभी पिछले दिनों मैने एक पोस्ट में महावीर अग्रवाल द्वारा लिये गये नामवर सिंह के साक्षात्कार का एक अंश प्रस्तुत किया था । पब्लिश होने के बाद जब मैने टिप्पणियाँ देखीं तो एक बेनामी टिप्पणी । मेरे तो हाथ पाँव फूल गये ,भई सीधे - सादे आदमी के घर एक अनजान आदमी मेहमान बन कर जबरन आ जाये तो उसकी हालत कैसी होगी बस वही मेरी हालत थी । सोचा टिप्पणी मॉडरेट कर दूँ.. अस्वीकार .. हाँलाकि यह बेनामी पढ़ा-लिखा तो दिखाई देता था और इस बहाने कई लोगो के मन मे उठ रहे प्रश्नों के जवाब भी दिये जा सकते थे । पसोपेश में था कि मुझे “ फोन ए फ्रैंड” का विकल्प याद आया सोचा मित्र से सम्वाद कर पूछ लूँ , पता नहीं यहाँ की क्या परम्पराएँ हैं ? क्या पता किसी से गलती से बेनामी वाले बॉक्स मे टिक हो गया हो और वास्तव में वह जानकारी चाहता हो .. उसके प्रश्न देखने से तो ऐसा ही लगता था ...
कल उड़न तश्तरी पर समीर भाई के सुभाषित का आनंद ले रहा था कि उनके एक सुभाषित पर नज़र पड़ी ..”प्रशंसा और आलोचना में वही फर्क है जो सृजन और विंध्वस में “ अरे.. मैने कहा यह तो मेरे ब्लॉग के काम की चीज़ है । याद आया अभी पिछले दिनों मैने एक पोस्ट में महावीर अग्रवाल द्वारा लिये गये नामवर सिंह के साक्षात्कार का एक अंश प्रस्तुत किया था । पब्लिश होने के बाद जब मैने टिप्पणियाँ देखीं तो एक बेनामी टिप्पणी । मेरे तो हाथ पाँव फूल गये ,भई सीधे - सादे आदमी के घर एक अनजान आदमी मेहमान बन कर जबरन आ जाये तो उसकी हालत कैसी होगी बस वही मेरी हालत थी । सोचा टिप्पणी मॉडरेट कर दूँ.. अस्वीकार .. हाँलाकि यह बेनामी पढ़ा-लिखा तो दिखाई देता था और इस बहाने कई लोगो के मन मे उठ रहे प्रश्नों के जवाब भी दिये जा सकते थे । पसोपेश में था कि मुझे “ फोन ए फ्रैंड” का विकल्प याद आया सोचा मित्र से सम्वाद कर पूछ लूँ , पता नहीं यहाँ की क्या परम्पराएँ हैं ? क्या पता किसी से गलती से बेनामी वाले बॉक्स मे टिक हो गया हो और वास्तव में वह जानकारी चाहता हो .. उसके प्रश्न देखने से तो ऐसा ही लगता था ... बेनामी ने कहा…
मुझे तो बिहारी में बहुत रस दिखता है। लगता है मेरी रस की ग्रन्थि सही नहीं है। कुछ सवाल है महोदय.....
1 रस में डुबने के लिये तुलसी के पास जाना पड़ेगा से नामवर जी का क्या तात्पर्य है, क्या इस लोक को छोड़ना पड़ेगा ?
2 आलोचक क्या होता है ? 3. ये मार्क्सवादी आलोचना क्या है? अन्य किस किस तरही की वादी आलोचनायें होती हैं ।
1 रस में डुबने के लिये तुलसी के पास जाना पड़ेगा से नामवर जी का क्या तात्पर्य है, क्या इस लोक को छोड़ना पड़ेगा ?
2 आलोचक क्या होता है ? 3. ये मार्क्सवादी आलोचना क्या है? अन्य किस किस तरही की वादी आलोचनायें होती हैं ।
मैने मित्र अशोक कुमार पाण्डेय से सम्पर्क किया । वे टिप्पणी देकर जा चुके थे लेकिन मेरे आग्रह पर फिर लौटकर आये । लेकिन वहाँ देखा तो दिनेशराय द्विवेदी जी पहले ही उस बेनामी की तलाशी ले चुके थे और उसे साफ साफ हिन्दी में समझा चुके थे ..कुछ इस तरह ..
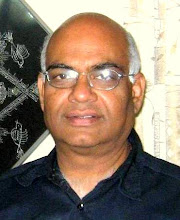 नामवर जी के उपरोक्त वक्तव्य से किसे आपत्ति हो सकती है? उन्हों ने जो कुछ कहा सच कहा। यूँ तो एक बात के अनेक अर्थ समझे जा सकते हैं। चाहें तो बेनामी जी ऊपर जाने के बजाय अपने पास के तुलसी के पौधे तक भी जा सकते हैं या फिर सीरियल वाली तुलसी तक भी। यहाँ तुलसी के पास जाने का अर्थ तुलसी साहित्य पढ़ने से है। मार्क्सवादी आलोचक से है मार्क्सवादी आलोचना से नहीं। खैर, जाकी रही भावना जैसी। वैसे उन की बात से असहमति हो तो यहाँ लिखा जा सकता है। आलोचना का महत्व इस बात से है कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की आलोचना लोगों की कृतियों को अधिक पाठकों तक पहुँचाती है। लेकिन बहुत लोग आलोचकों को पसंद ही नहीं करते ।
नामवर जी के उपरोक्त वक्तव्य से किसे आपत्ति हो सकती है? उन्हों ने जो कुछ कहा सच कहा। यूँ तो एक बात के अनेक अर्थ समझे जा सकते हैं। चाहें तो बेनामी जी ऊपर जाने के बजाय अपने पास के तुलसी के पौधे तक भी जा सकते हैं या फिर सीरियल वाली तुलसी तक भी। यहाँ तुलसी के पास जाने का अर्थ तुलसी साहित्य पढ़ने से है। मार्क्सवादी आलोचक से है मार्क्सवादी आलोचना से नहीं। खैर, जाकी रही भावना जैसी। वैसे उन की बात से असहमति हो तो यहाँ लिखा जा सकता है। आलोचना का महत्व इस बात से है कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की आलोचना लोगों की कृतियों को अधिक पाठकों तक पहुँचाती है। लेकिन बहुत लोग आलोचकों को पसंद ही नहीं करते ।मैने सोचा बेनामी पढ़ा लिखा भले न हो ,लिखा_पढ़ा , मतलब लेखक प्रजाति का होगा तो द्विवेदी जी की बात समझ जायेगा , लेकिन अशोक जी ने इतनी गम्भीरता से यह समझाया था कि मुझे उन्हे प्रस्तुत करना ज़रूरी लगा , सो लीजिये आप भी पढ़िये बेनामी जी के सवाल के यह महत्वपूर्ण जवाब ।
वैसे तो बेनामी होकर की गयी बात को गंभीरता से लेने का जी नहीं करता। फिर भी चूंकि सवाल हैं और गम्भीर हैं तो जवाब देना ही है--
1] अब आपकी रस ग्रन्थि के बारे में आप ही फ़ैसला कीजिए। आपने ख़ुद लिखा है कि बिहारी में आपको रस दिखाई देता है। तो यह नामवर जी से अलग क्या है? वह भी शुक्ल जी के हवाले से यही कह रहे हैं कि जिन्हें रस का आस्वादन नक्काशी की तरह (आशय ऊपरी सजावट से है) करना है उसके लिये निश्चित तौर पर बिहारी काफ़ी हैं। लेकिन रस का आस्वादन करना है, उसमें डूबना है उसे कविता के भीतर प्रवेश करना होगा। ऐसे में कविता की आत्मा उसके लिये एक आवश्यक संघटक तत्व है। एक ऐसा आंतरिक सौन्दर्य जो कविता को बहुअर्थी तो बनाता ही है, साथ ही अपने अंतस में एक ऐसा स्पेस बनाता है जहां तक पहुंच कर पाठक कविता के साथ एकाकार होता है। इसके लिये कविता की अपने समय और जन के साथ एक अनन्य सहानूभूति ज़रूरी है। यही विभेद कबीर या तुलसी से बिहारी को अलग करता है।
2) अब आलोचक क्या होता है यह सवाल मुझे तो अजीब लगता है। फिर भी आलोचक अपने समय तथा समाज को समझने वाला ऐसा विशेषज्ञ होता है जो कविता को पुनर्प्रस्तुत करता है। वह अपने समय की कसौटी पर कविता को कसता है। लोग आलोचक को लेकर अक्सर कुछ ज़्यादा ही असहिष्णु होते हैं। अब अगर यह पूछा जाये कि बिहारी हों या कबीर या फिर तुलसी हों अगर उनके अध्येताओं ने आधुनिक समय में उनको फिर से पढकर पुनर्प्रस्तुत और पुनर्व्याख्यायित नहीं किया होता तो क्या केवल स्मृतियों और चन्द पाण्डुलिपियों के भरोसे उनको इस तरह समग्र में पढ पाना संभव होता?
3]मार्क्सवादी आलोचना एक वैज्ञानिक पद्धति के सहारे कविता को समझने तथा व्याख्यायित करने का उन्नत औज़ार है। यह उस भौतिकवादी अवधारणा के आधार पर कविता की व्याख्या करती है जो जीवन की भाववादी अवधारणा को ख़ारिज़ करती है। यानि वह विचार जो मानता है कि कोई इश्वरीय प्रेरणा रचना नहीं करवाती और न ही कोई कवि बन कर पैदा होता है। एक आदमी अपने चतुर्दिक संसार के अनुभवों से सीखता है और इस सामाजिक संपत्ति , ज्ञान और परिवेश जनित संवेदना के सहारे अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है…कविता उनमें से एक है। आप इस दर्शन की जडें भारतीय दर्शन की परम्परा में तलाश सकते हैं। यह पद्धति भी कविता को कलाकर्म ही मानती है लेकिन साथ ही वह कला के सामाजिक सरोकारों को भी मान्यता देती है।
उदाहरण दूं तो इस मानवविरोधी दौर में अगर एक गीत ऐसा लिखा जाये जो किसानों की आत्महत्या की बात का मज़ाक उडाये और खेती बारी के दुश्मनो की प्रशंसा के गीत गाये ( जैसे गुलामी के दौर में अंग्रेज़ों के समर्थन में लिखे गीत) तो मार्क्सवादी पद्धति का सही आलोचक उसको रेशा-रेशा खोलकर साबित करेगा कि यह गीत ख़ारिज़ करने योग्य है। इसके उलट आत्महत्याओ के संताप से आतुर जो गीत इस हालात को बदलने की बात करेगा उसे यह पद्धति आगे ले आयेगी।
अब मार्क्सवादी आलोचकों ने किया कि नहीं यह एक अलग बात है। इसे लेकर भी तमाम असहमतियां हैं मेरी।
रहा सवाल दूसरी पद्धतियों का तो भाई भाववादी आलोचना की भी एक पद्धति है…आप चाहें तो एक आह-वाह वादी आलोचना भी है…जनविरोधी और दक्षिणपंथी आलोचना पद्धति है…पर ये आपकी तरह बेनामी होके ही आना पसंद करते हैं। देखिये ना प्रतिबद्धता का मतलब मार्क्सवाद से प्रतिबद्धताओं को ही मान लिया जाता है। संघ के और दूसरी विचारधाराओं के हिमायती शायद केवल अवसरवाद से ही संबद्ध होते हैं प्रतिबद्धता से नहीं ।
1] अब आपकी रस ग्रन्थि के बारे में आप ही फ़ैसला कीजिए। आपने ख़ुद लिखा है कि बिहारी में आपको रस दिखाई देता है। तो यह नामवर जी से अलग क्या है? वह भी शुक्ल जी के हवाले से यही कह रहे हैं कि जिन्हें रस का आस्वादन नक्काशी की तरह (आशय ऊपरी सजावट से है) करना है उसके लिये निश्चित तौर पर बिहारी काफ़ी हैं। लेकिन रस का आस्वादन करना है, उसमें डूबना है उसे कविता के भीतर प्रवेश करना होगा। ऐसे में कविता की आत्मा उसके लिये एक आवश्यक संघटक तत्व है। एक ऐसा आंतरिक सौन्दर्य जो कविता को बहुअर्थी तो बनाता ही है, साथ ही अपने अंतस में एक ऐसा स्पेस बनाता है जहां तक पहुंच कर पाठक कविता के साथ एकाकार होता है। इसके लिये कविता की अपने समय और जन के साथ एक अनन्य सहानूभूति ज़रूरी है। यही विभेद कबीर या तुलसी से बिहारी को अलग करता है।
2) अब आलोचक क्या होता है यह सवाल मुझे तो अजीब लगता है। फिर भी आलोचक अपने समय तथा समाज को समझने वाला ऐसा विशेषज्ञ होता है जो कविता को पुनर्प्रस्तुत करता है। वह अपने समय की कसौटी पर कविता को कसता है। लोग आलोचक को लेकर अक्सर कुछ ज़्यादा ही असहिष्णु होते हैं। अब अगर यह पूछा जाये कि बिहारी हों या कबीर या फिर तुलसी हों अगर उनके अध्येताओं ने आधुनिक समय में उनको फिर से पढकर पुनर्प्रस्तुत और पुनर्व्याख्यायित नहीं किया होता तो क्या केवल स्मृतियों और चन्द पाण्डुलिपियों के भरोसे उनको इस तरह समग्र में पढ पाना संभव होता?
3]मार्क्सवादी आलोचना एक वैज्ञानिक पद्धति के सहारे कविता को समझने तथा व्याख्यायित करने का उन्नत औज़ार है। यह उस भौतिकवादी अवधारणा के आधार पर कविता की व्याख्या करती है जो जीवन की भाववादी अवधारणा को ख़ारिज़ करती है। यानि वह विचार जो मानता है कि कोई इश्वरीय प्रेरणा रचना नहीं करवाती और न ही कोई कवि बन कर पैदा होता है। एक आदमी अपने चतुर्दिक संसार के अनुभवों से सीखता है और इस सामाजिक संपत्ति , ज्ञान और परिवेश जनित संवेदना के सहारे अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है…कविता उनमें से एक है। आप इस दर्शन की जडें भारतीय दर्शन की परम्परा में तलाश सकते हैं। यह पद्धति भी कविता को कलाकर्म ही मानती है लेकिन साथ ही वह कला के सामाजिक सरोकारों को भी मान्यता देती है।
उदाहरण दूं तो इस मानवविरोधी दौर में अगर एक गीत ऐसा लिखा जाये जो किसानों की आत्महत्या की बात का मज़ाक उडाये और खेती बारी के दुश्मनो की प्रशंसा के गीत गाये ( जैसे गुलामी के दौर में अंग्रेज़ों के समर्थन में लिखे गीत) तो मार्क्सवादी पद्धति का सही आलोचक उसको रेशा-रेशा खोलकर साबित करेगा कि यह गीत ख़ारिज़ करने योग्य है। इसके उलट आत्महत्याओ के संताप से आतुर जो गीत इस हालात को बदलने की बात करेगा उसे यह पद्धति आगे ले आयेगी।
अब मार्क्सवादी आलोचकों ने किया कि नहीं यह एक अलग बात है। इसे लेकर भी तमाम असहमतियां हैं मेरी।
रहा सवाल दूसरी पद्धतियों का तो भाई भाववादी आलोचना की भी एक पद्धति है…आप चाहें तो एक आह-वाह वादी आलोचना भी है…जनविरोधी और दक्षिणपंथी आलोचना पद्धति है…पर ये आपकी तरह बेनामी होके ही आना पसंद करते हैं। देखिये ना प्रतिबद्धता का मतलब मार्क्सवाद से प्रतिबद्धताओं को ही मान लिया जाता है। संघ के और दूसरी विचारधाराओं के हिमायती शायद केवल अवसरवाद से ही संबद्ध होते हैं प्रतिबद्धता से नहीं ।
तो अब तक उन बेनामी जी की समस्या का समाधान हो गया होगा इसलिये वे दोबारा नहीं आये लेकिन अलबेला भाई जाते जाते एक फुलझड़ी छोड़ ही गये ।
साधुवाद इस उम्दा पोस्ट के लिए..........
वैसे कहना नहीं किसी से, अपनी आलोचकों से पटती नहीं है
अरे भाई प्रशंसक जो प्यारे लगते हैं..........हा हा हा
वैसे कहना नहीं किसी से, अपनी आलोचकों से पटती नहीं है
अरे भाई प्रशंसक जो प्यारे लगते हैं..........हा हा हा
मैं क्या जवाब देता उनका यह गम्भीर मज़ाक हँसाने के लिये ही था सो हँस लिया फिर भी कुछ तो कहना ही था सो ..एकदम सीरियसली कहा ..
@अलबेला भाई, आलोचना का अर्थ केवल निन्दा नहीं होता है ,प्रशंसा भी होता है ( विस्तार के लिये पढ़ें अशोक जी का जवाब क्र. 2) वैसे आप भी किसी से कहना नहीं ..लेखक लिखेगा ही नहीं तो आलोचक क्या खाक आलोचना करेगा ..हा हा हा ।
आप भी इसी परिप्रेक्ष्य में अपने मन में उठ रहे सवालों के उत्तर इस सम्वाद में ढूंढिये और अपनी पोस्ट पर मेरी टिप्पणियों का बुरा मत मानिये । कुल मिलाकर हम सभी का प्रयास यही है ना कि ब्लॉग जगत में स्तरीय साहित्य की प्रस्तुति करें । द्विवेदी जी, अशोक भाई ,समीर भाई , अलबेला भाई और अन्य सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापिता करते हुए - आपका शरद कोकास

